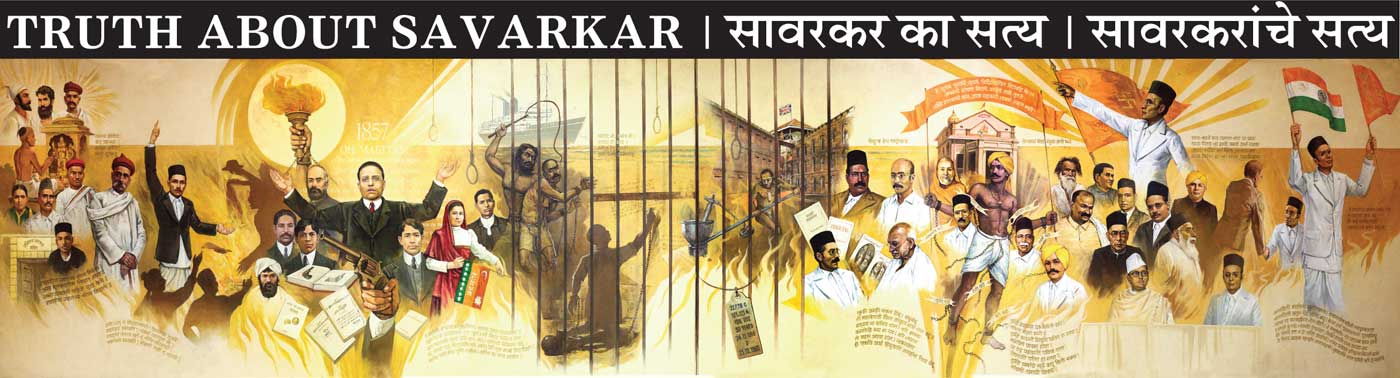आरोप
स्वातंत्र्यवीर सावरकर अंदमान जेल जाने के बाद मानसिक रूप से परेशान थे और उन्होंने एक के पीछे एक माफीनामें भेजे, यह बात सबसे छुपाकर रखी गई।इसी प्रकार उन्हें कोल्हू आदि चलाने की कठोर यातनाये नहीं दी गयी।
वस्तुस्थिति
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यूरोप और रशिया में घटित अनेक क्रांतियों का अध्ययन करके भारत में क्या और कैसे कार्य करना चाहिए इसका अंदाजा प्राप्त कर चुके थे। गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा जाए इसका मार्गदर्शन युवकों को मिले, इस उद्देश्य से इटली की क्रांति के जनक जोसफ मैजिनी की आत्मकथा का अनुवाद सावरकर ने १९०६ में लंदन पहुंचते ही कर दिया था। इस पुस्तक में सावरकर द्वारा लिखी गई प्रस्तावना क्रांतिकारियों के लिए गीता ही सिद्ध हुई।
जोसेफ मैजिनी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। सावरकर के समान उन्होंने भी कुछ शर्तों को स्वीकार करके अपने आपको मुक्त करा लिया। परंतु, इस के पश्चात भी जोसफ मैजिनी को इटली का श्रेष्ठ क्रांतिकारी माना जाता है; और उसी इटली से आई एक महिला और उसके बच्चे सावरकर को क्षमायाचना वीर कहकर अपमानित करते हैं।
शक्ति हो तो वे इटली जाकर जोसेफ मैजिनी को क्षमायाचना वीर कहने की शक्ति दिखाएं।नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भी अंग्रेजों की कुछ शर्तें मानकर अपने आपको छुड़ावाया था। क्या अब उनको भी आप माफिवीर कहेंगे?
सावरकर ने क्षमायाचना की यह सरासर झूट मुद्दा लेकर सावरकर को हमेशा बदनाम किया जाता है। लेकिन क्या उनकी याचिकाए मफिपत्र थे?
अपनी मांग के लिए लिखित याचिका करने का अधिकार प्रत्येक कैदी को होता है और उन लिखित याचिकाओं को ‘दया याचिका- मर्सी पिटिशन’ के नाम सेही संबोधित किया जाता है। दया याचिका करना मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन फांसी की सजा पाए कैदी इन याचिकाओं को नहीं कर सकते थे। इसलिए फांसी की सजा पाए किसी कैदी ने ऐसी याचिका नहीं की थी।
सावरकर अंदमान पहुंचे तो उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय, सुविधाएं मिलने और सभी क्रांतिकारियों की मुक्ति के लिए कई याचिकाएं की। ये जानकारियां उन्होंने छिपाई नहीं बल्कि अपनी आत्मकथा ‘मेरा आजीवन कारावास’ में उद्धृत की हैं। लेकिन इन आवेदनों में सावरकर ने कहीं भी अपने किये पर क्षमा नहीं मांगी और पश्चाताप व्यक्त नहीं किया।
सावरकर बैरिस्टर थे इसलिए अधिवक्ता की दृष्टि से उन्होंने छूटने के लिए नैर्बधिक प्रयास किये। इसमें गलत क्या था? क्या सावरकर और अन्य क्रांतिकारी अदमान में ही मर जाएं यह काँग्रेसियों की विकृत आकांक्षा थी?
सावरकर का मत था किसी भी प्रकार अंग्रेजों के बंदिवास से मुक्त होकर पुन: क्रांति का कार्य शुरू करना यह प्रत्येक क्रांतिकारी का कर्तव्य है। सावरकर अपना ये मत अंदमान में मौजूद क्रांतिकारियों के समक्ष कई बार रखते थे। महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ संन्याल को लाहौर षड्यंत्र के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, वे भी सावकर की भांति वचन पत्र देकर मुक्त हुए थे। उन्होंने पुन: तिव्र गति से क्रांति कार्य शुरू किया और प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र के सूत्रधार के रूप में उन्हें पुन: आजीवन कारावास की सजा भी हुई। अपनी ‘बंदी जीवन’ नामक आत्मकथा के पृष्ठ २२६ में वे कहते हैं,“सावरकर ने मेरी तरह याचिका की थी।परन्तु मुझे मुक्ति मिली, लेकिन उन्हें नहीं; क्योंकि शासन को डर था कि सावरकर छूटे तो महाराष्ट्र में पुन: विद्रोह का विस्फोट होगा।”
सावरकर ने कई याचिकाएं की लेकिन, उन्होने कहीं भी पश्चाताप या क्षमा याचना नहीं की। उनका १९१३ का आवेदन तो उन्हे सामान्य बंदिवानों को जो सुविधाये मिळती है उनसे उन्हे तथा अन्य क्रांतीकारियो को वंचित रखने के विरुद्ध था।सामान्य बंदिवानों को मात्र छह महिने सेल्युलर कारागृह मे रखने के पश्चात बाहर द्वीप पर खुले कारावास मे रखते थे।अन्य क्रांतीकारियो को एक-दीड वर्ष के पश्चात बाहेर भेजा गया।मात्र सावरकर ऐसे अकेले बंदी थे जिन्हे अपने रिहाई के अंतिम दिन तक, याने की १४ साल तक, कोठरी-बंद रखा था।अंदमान आने के पश्चात बंदियो को सेल्युलर कारागृह में छह मास रखने का नियम था, परंतु सावरकर को तो छह महिने एकांतवास मे रखा गया।इतना प्रदीर्घ एकांतवास मानसिक रूप से कितनी भयंकर पिडा देता है यह कहने की आवश्यकता नही!१९१३ की याचिका में उनकी मांग थी की हमें या तो राजनीतिक कैदी का दर्जा दो, या सामान्य कैदी जैसी सुविधाएं दो; और यदि ये संभव न हो तो भारत या बर्मा की जेल में भेज दो। इस याचिका में सावरकर ने अंग्रेजों पर क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ऐसा आरोप कोई क्षमा याचना में करेगा क्या?
अक्तूबर १९१४ में विश्व युद्ध की पार्श्वभूमि पर लिखी गई याचिका के अंत में वे लिखते हैं,“मैंने जो लिखा है, इस विषय में सरकार के मन में शंका हो तो मुझे बिल्कुल मुक्त न करे लेकिन, अन्य सभी को तो छोड़ दें।”
५ अगस्त १९१७ की याचिका के अंत में सावरकर लिखते हैं,“यदि सरकार को लग रहा हो कि ये सब मैं अपनी मुक्ति के लिए लिख रहा हूं या सभी की मुक्ति में मेरा नाम ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा हो तो मेरा नाम काट दें। मुझे अपनी मुक्ति से जितना समाधान मिलेगा उतना ही समाधान अन्य लोगों के छूटने से भी मिलेगा। इन राजनीतिक बंदियों के साथ अपनी मातृभूमि के लिए भूमिगत हुए, बिछड़े क्रांतिकारियों को भी वापस लौटने का अवसर मिले।”
अंग्रेजों के दस्तावेज में इन याचिकाओं को स्पष्टरूप से “Petition for General Amnesty for all the political prisoners”ऐसा संबोधित किया गया है।इसका अर्थ स्पष्ट है, ये आवेदन सभी राजनैतिक बंदियों के लिए थे!
स्वातंत्र्यवीर सावरकर जेल गए थे या नहीं और सावरकर की मुक्ति याचिका उनकी व्यूहरचना का हिस्सा थी या नहीं ये देखना हो तो उसके लिए उनके साथ सजा भुगत रहे क्रांतिकारियों और जेल डायरी की जांच आवश्यक है। सावरकर के साथ जेल में रहे क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त, भाई परमानंद, पृथ्वीसिंह आजाद और रामचरणलाल शर्मा नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा उनकी आत्मकथाओं में किया गया सावरकर का उल्लेख वस्तुस्थिति को स्पष्ट करनेवाला है।
उल्लासकर दत्त को अति प्रताड़ना के कारण मनोरोग का झटका आया था। इसके पहले जब उन्हें हथकड़ी में टांगकर रखा गया था तब उन्हें ज्वर का आभास हुआ। इस पर जेल अधिकारी बारी ने उन्हें द्वंद युद्ध का आह्वान दिया था उनके बदले सावरकर ने युद्ध किया और बारी का पराभव किया। (12 years in prisonline – page ६४-६५) पूर्णत: भ्रम की स्थिति में होने के बावजूद सावरकर ही मेरे लिए लड़ने के योग्य हैं, उल्लासकर दत्त के इस विश्वास से सावरकर का मनोबल १९१२ में कैसा था, यह सिद्ध होता है।
१९१३ में ‘सुराज्य’ समाचार पत्र के संपादक रामचरणलाल शर्मा को काम बंद आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए जब जेल अधिकारी ने सजा बढ़ाने की धमकी दी तब उन्होंने उत्तर दिया,“यदि विनायक सावरकर ५० वर्ष काट सकते हैं, तो मैं भी काट लूंगा।” (कालापानी का ऐतिहासिक दस्तावेज पृष्ठ ५३) अर्थात १९१३ में भी क्रांतिकारी, सावरकर की ओर एक आदर्श की दृष्टि से देख रहे थे।
१९१९ के बंद के लिए अंदमान में सजा भुगत रहे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद अपनी आत्मकथा ‘आपबीती’ में लिखते हैं कि, जेल में होनेवाले सभी संघर्षों के लिए जेल अधिकारी बारी और पर्यवेक्षक, सावरकर बंधुओं को जिम्मेदार मानते थे। (आपबीती – पृष्ठ १०२)
१४ नवंबर १९१३ में याचिका करते हुए सावरकर ने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक से निजी चर्चा की थी। ये याचिका सरकार के पास भेजते समय २३ नवंबर १९१३ की रिपोर्ट में सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक ने सावरकर के बारे में जो निष्कर्ष निकाले थे वह महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं:
“…सावरकर की दया याचिका में उन्होंने उसमें कहीं भी खेद या ग्लानि व्यक्त नहीं की है लेकिन, उन्होंने अपने दृष्टिकोण में बदलाव का दावा किया है। उनका कहना है कि १९०६-१९०७ की बदली परिस्थिति के कारण उन्होंने षड्यंत्र रचा। उनका विचार है कि अब सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली, शिक्षा आदि के विषय में सुधार करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है इसलिए क्रांतिकारी मार्ग के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है।
“… सावरकर के विषय में यहां कोई छूट देना संभव नहीं है और मेरे मत से वे किसी भी भारतीय जेल से भाग जाएंगे। वे इतने महत्वपूर्ण नेता हैं कि यूरोप के अराजकतावादी भारतीय उन्हें मुक्त कराने के लिए षड्यंत्र रचकर उसे अल्पकाल में ही अमल में भी ला देंगे। उन्हें यदि सेल्यूलर जेल के बाहर अंदमान में रखा गया तो उनका छूटना निश्चित है। उनके मित्र सहजता से कोई नौकाकिराये से लेकर आस-पास के किसी छोटे द्वीप पर छुपा सकते हैं और कुछ पैसे खर्च करने के पश्च्यातअन्य बाकी सभी चीजें सहज संभव होगी।
“…सावरकर जैसे मानव के लिए अनगिनत काल तक कठोर परिश्रम का कार्य देना संभव नहीं है। एक के बाद एक पचास साल की सजा ही उन्हें जीवनभर जेल में रखने के लिए पूरी है। कुछ वर्षों की कठोर परिश्रमवाली सजा उनके अपराध के दंड के रूप में ठीक है और वे समाज के लिए खतरा हैं इसलिए बचे हुए काल भी उन्हें जेल में ही बिताना पड़ेगा।”
सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक का ये निष्कर्ष अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग द्वारा अगस्त १९१३ में दी गई रिपोर्ट के आधार पर था। B-August 1913 no.61 की इस रिपोर्ट में मैडम कामा के अदमान में बंद स्वातंत्र्यवीर सावकर और अमेरिका, जर्मनी के क्रांतिकारियों के निरंतर संपर्क में होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
२३ नवंबर १९१३ को क्रांतिकारियों और जर्मन सरकार के बीच बिचौलिया बनकर कार्य करनेवाले एक शख्स को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मिले दस्तावेजों में सेल्युलर जेल पर हमला करके क्रांतिकारियों को छुड़ाने और उनके नेतृत्व में ब्रम्हदेश (म्यांमार) में विद्रोह करने की योजना का पूरा ब्यौरा था। इसके लिए सैकड़ों क्रांतिकारी ब्रम्हदेश (म्यांमार) में एकत्रित हो गए थे। इस दस्तावेज में अंदमान द्वीप और सेल्यूलर जेल का नक्शा, वहां काम करनेवाले अधिकारियों का नाम तथा सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत जानकारी थी। सेल्यूलर जेल में से जिन्हें मुक्त कराना था उसमें पहला नाम था सावरकर बंधुओं का।
क्रांतिकारियों को मुक्त कराने के लिए सर्वप्रथम जर्मनी की एम्डेन नौका ने १९१४ में अंदमान की नाकेबंदी की। लेकिन उसी समय अंग्रेजों की ‘एचएमएस सिडनी’ नामक अधिक-उन्नत युद्धनौका ने एम्डेन पर हमला करके उसे कोको द्वीप के पास डुबो दिया।
रासबिहारी बोस के निकटवर्तीय सहयोगी सच्चिंद्रनाथ संन्याल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रासबिहार बोस ने एक और नौका दिसंबर १९१५ में अंदमान की तरफ भेजी थी। इस बार हिंदुस्थानी क्रांतिकारियों को निकोबार द्वीप पर उतारकर रात में अंदमान पर हमला करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त दो नौकाएं युद्ध की सामग्री के साथ भारत की तरफ रवाना हुई थीं। लेकिन इस योजना की संपूर्ण जानकारी अंग्रेज गुप्तचर विभाग को मिल जाने के कारण युद्ध सामग्री ले जा रही एक नौका को उन्होंने जब्त कर लिया। दूसरी नौका का क्या हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन एचएमएस कॉर्नवाल नामक अंग्रेजों की नौका ने दिसंबर १९१५ के अंतिम सप्ताह में अंदमान की तरफ जानेवाली नौका डुबा दी थी। इसी समय शस्त्रास्त्र लेने के लिए निकले बंगाल के क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय (बाघा जतीन) को सितंबर १९१५ में बालासोर में दो साथियों के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया।
इसी समय भारतीय सेना में विद्रोह करने की योजना का भी खुलासा हुआ। विष्णू गणेश पिंगले ने रासबिहारी बोस, सच्चिंद्रनाथ संन्याल, कर्तारसिंह सराबा के सहयोग से विद्रोह करने की बड़ी योजना बनाई थी। अंग्रेजों ने इंडियन डिफेन्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके क्रांतिकारी पिंगले और कर्तार सिंह के साथ अन्य पाच क्रान्तिकारियो को फांसी की सजा दे दी। अन्य क्रांतिकारियों को लंबी अवधि की सजा के लिए अंदमान भेज दिया।
ब्रम्हदेश (म्यांमार) में सक्रिय सात क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई जबकि आठ लोगों को आजीवन कारावास के लिए अंदमान में बंद कर दिया गया।
भारत में विद्रोह का बिगुल फूंककर उसी समय ब्रम्हदेश (म्यांमार) से भारत पर आक्रमण करने की ये महत्वाकांक्षी योजना थी। ये भारत और विदेश के क्रांतिकारी संगठनों की एकजुटता में सबसे बड़ी मुहिम थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्वातंत्र्यवीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों को अंदमान से छुड़ाकर सयाम (थाईलैंड) ले जाना था और उन्हीं के नेतृत्व में पहले सयाम और बाद में बर्मा को कब्जे में लेकर भारत पर सीधा आक्रमण करना था।
दुर्भाग्यवश इस योजना में अपयश मिला फिर भी ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए कार्यरत् अनगिन बेनाम क्रांतिकारी देश कल्याण के लिए लग गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके परिवार और उनका क्या हुआ इसकी साधारण चर्चा तक भी नहीं थी। हजारो युवा कभी वापस लौटे ही नहीं, उनकी खबर तक उनके परिजनों के नसीब थी।हजारों वीर माताएं, वीर पत्नीया हमारे पुत्र, हमारे पति कब वापस लौटेंगे इसका इंतजार करती रहीं और दरवाजे पर होनेवाली प्रत्येक थाप उनकी अपेक्षाओं को भंग करती रही!
आज इतनी महत्वपूर्ण योजना की, क्रांतिकारियों के बलिदान की और इन वीर माताओं एवम वीर पत्नियों के असाधारण त्याग की जानकारी तक किसी को न हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गुण गाए जा रहे हैं केवल राज प्रसाद में सुख का उपभोग करनेवाले बंदियों के! पत्नी के बीमार होने के बावजूद, अपने दुराग्रह के कारण उसका आधुनिक इलाज न करने देनेवाले, उसे मौत के मुंह में धकेलनेवाले तथाकथित महात्माओं और उनकी विकृत सत्ता के प्रयोगों के!!
अंग्रेजों की सभी रिपोर्ट यही सिद्ध करती है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर अंदमान में अमानवीय यातना भोगते हुए भी युरोप, अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता से क्रांति की योजनाएं रच रहे थे।
सावरकर ने और उनके बंधु नारायण राव द्वारा किए गए आवेदनों के कारण ही, सावरकर बंधुओं को छोड़कर अन्य क्रांतिकारियों को कुछ सुविधाएं मिलीं, सैकड़ों क्रांतिकारियों को रिहाई मिली जबकि सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए वर्ष १९२१ तक इंतजार करना पड़ा। तब तक वीर सावरकर को कोई भी छूट अंग्रेजों ने नहीं दी और न ही उनकी कोठरी बंदी में कोई कमी हुई।
अंदमान से छूटा प्रत्येक क्रांतिकारी राजनीति में हिस्सा न लेने की शर्त मानकर ही छूटा है। १९३१ में कांग्रेसी नेताओं पर चल रहे सभी मामले वापस लें, इस शर्त पर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन ही गांधी-नेहरू ने वापस ले लिया था और १९३५ में जेल से छूटते समय ऐसी ही शर्त नेहरू ने भी स्वीकार की थी।
अब इतना होने के पश्चात भी मात्र राजनीति में हिस्सा न लेने की शर्त मानकर छूटे इसलिए सावरकर को माफी वीर कहोगे क्या?
सावरकर ने जेल में कोई कष्ट नहीं भोगे, ऐसा निराधार आरोप कुछ लोग करते हैं। लेकिन अंदमान में १९१६ से १९२१ के मध्य सजा भुगत रहे महान क्रांतिकारी पृथ्वीसिंह आजाद का अनुभव कुछ और ही कहता है।
“वीर सावरकर ने आधुनिक भारत के युवकों को क्रांति का पाठ पढ़ाया था। क्रांतिकारी वृत्तिवाले नवयुवकों के वे तेजस्वी नेता थे। ऐसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति से अंग्रेज अधिकारियों ने वह काम लिया जो बैलों से लिया जाता था। तेल के कोल्हू पर प्रतिदिन तीस पाउंड तेल निकालने के लिए सावरकर को मजबूर किया गया।”(क्रांति के पथिक – पृष्ठ १०८)
पृथ्वीसिंह आजाद के भारत वापस आने के बाद, अंग्रेजों की कैद से छूटे स्वातंत्र्यवीर सावरकर के छोटे बंधु नारायण राव सावरकर ने ही उन्हें आसरा दिया था (क्रांति के पथिक – पृष्ठ १५३)। इसके बाद भगतसिंह को फांसी की सजा सुनाने के बदले के स्वरूप में पृथ्वीसिंह आजाद और सुप्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी वोरा ने जब १९३० में लैमिंग्टन पुलिस थाने पर गोलाबारी की, उस समय उनके साथ स्वातंत्र्यवीर सावरकर के विश्वसनीय साथी और क्रांतिकारी गणेश रघुनाथ वैशंपायन भी थे। (क्रांति के पथिक – पृष्ठ १९०)
अर्थात पृथ्वीसिंह आजाद, उल्हासकर दत्त, भाई परमानंद, रामचरणलाल शर्मा और सच्चिंद्रनाथ संन्याल के जैसे महान क्रांतिकारियों का अनुभव झूठा है, ऐसा सावरकर विरोधियों को कहना है क्या?
वर्तमान में उपलब्ध सावरकर के कारागृह के रिकॉर्ड से स्वातंत्र्यवीर सावरकर को सुनाई गई अमानवीय सजा और सावरकर के व्यवहार की जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें कोल्हू पेरने का रेकॉर्ड नहीं है, इसलिए सावरकर ने कोल्हू चलाया ही नहीं ऐसा आरोप कुछ किराए के लेखक करते हैं। लेकिन कोल्हू पेरना ये नियमित कार्य था, सजा नहीं, इसलिए इस उल्लेख का यहां न होना स्वाभाविक है। अंग्रेज गृहमंत्री सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक ही यह कहते हैं।
अब क्या-क्या सजा सावरकर को हुई वो देखें और यह भी देखे की कैसा निडर था उनका आचरण!
- जेल में पहुंचने के ११वें दिन दिनांक १५ जुलाई १९११ को छह महीने के लिए कोठरी में बंद कर दिया गया।
- १५ जनवरी १९१२ को उनका कोठरी वास खत्म हुआ।
- ११ जून १९१२ को उनके पास कागज मिलने के बाद एक माह एकांतवास
- १९ सितंबर १९१२ को उनके पास से दूसरे को लिखा गया पत्र मिलने के बाद सात दिन की खड़ी हाथबेड़ी
- २३ नवंबर १९१२ को उनके पास दूसरे को लिखा गया पत्र मिलने के बाद एक माह एकांतवास की सजा।
- ३० दिसंबर १९१२ से २ जनवरी १९१३ की कालावधि तक अन्न त्याग
- १६ नवंबर १९१३ को रेजिनॉल्ड क्रेडॉक से भेंट के पश्चात काम नकारने के कारण एक महीने के एकांतवास की सजा।
- ८ जून १९१४ को काम करने से नकार देने के कारण सात दिन हाथ बेड़ियां पहनकर खड़े रहने की सजा।
- १६ जून १९१४ को काम करने से नकारने के बाद चार महीने जंजीरों से जकड़ेजाने की सजा
- १८ जून १९१४ को काम करने से पूर्ण नकार के पश्चात दस दिन खड़े बेड़ियों की सजा
स्वातंत्र्यवीर सावरकर को दी गईं कई सजा अवैध होने के कारण उसका लिखित उल्लेख नहीं किया गया ऐसा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने ‘माझी जन्मठेप’ नामक पुस्तक में स्पष्टता से कहा है। अन्य क्रांतिकारियों की आत्मकथाओं से भी वह प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त अधूरा दस्तावेज देखने के बाद भी सावरकर को कितनी कठोर सजा मिली थी, इसकी झलक मिलती है। अंदमान पहुंचते ही सावरकर को तुरंत ६ महीना एकांतवास में रखा गया था। ये सजा कितनी कठोर और अमानवीय है इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है।
स्वातंत्र्यवीर सावरकर का जेल में व्यवहार कैसा था इस बारे में १९१९ में एक रिपोर्ट कहती है “उनका व्यवहार नम्र हो तब भी उन्होंने सरकार से सहकार्य करने की प्रवृत्ति कहीं भी नहीं दिखाई। उनकी राजनीतिक सोच क्या है, ये इस समय कहना कठिन है।” सावरकर अब भी खतरनाक कैदी हैं इसलिए सावरकर को सर्वत्र माफी का लाभ न दिया जाए, ये निर्णय मुंबई प्रांतीय सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर लिया था।
रेजिलॉल्ड क्रेडॉक के समक्ष तथाकथित प्रार्थना पत्र सादर करने के पश्चात ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर तुरंत काम बंद करते हैं और इसके लिए उन्हें एक महीने की एकांतवास की सजा होती है, और उसके बाद भी कई बार काम करने से इन्कार करने के कारण वे खड़ीबेड़ी, डंडाबेड़ी, एकांतवास की शिक्षा भोगते हैं;ये उनके दृढ़ स्वभाव का निर्विवाद दर्शन है।
इसके बाद भी सावरकर के मनोबल को लेकर किसी के मन में कोई शंका होगी तो उसका निराकरण करनेवाला विश्वसनीय प्रमाण स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को मिल गया है। अंदमान में स्वातंत्र्यवीर सावरकर द्वारा हस्तलिखित दस्तावेज प्रकाश में आया है उसमें स्वातंत्र्यवीर सावरकर द्वारा उर्दू में लिखी गई तीन रचनाएं हैं। १९२१ की हस्तलिखित ये तीन रचनाएं युवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का अह्वान करती हैं। इसमें से एक गीत सच्चिंद्रनाथ संन्याल के माध्यम से काकोरी षड्यंत्र के आरोपियों तक पहुंचा होगा। जेल में क्रांतिकारी देश भक्ति पर जो गीत गाते थे उसमें सावरकर की ‘यही पाओगे…’ नामक गजल सम्मिलित थी। (काकोरी के दिलजले, पृष्ठ ११२) सावरकर अपनी एक रचना में कहते हैं,
हंता रावण का है अपना राम वीरवर सेनानी,
कर्मयोग का देव है स्वयं कृष्ण सारथी अभिमानी।
भारत तेरे रथ को सेना कौन रोकनेवाली हैं,
फिर देर क्यूं, उठो भाई हम ही हमारे वाली हैं।।
१९१० में अंदमान जाने से पहले लिखी गई “पहिला हप्ता” नामक कविता में यही भाव व्यक्त हुआ था और ११ वर्ष के कठोर कारावास के बाद भी सावरकर का विचार किंचित मात्र भी बदला नहीं था, सावरकर की इसी हस्तलिखित रचना से निर्विवादिता सिद्ध होती है।
स्वातंत्र्यवीर सावरकर की छूटने को लेकर स्पष्ट भूमिका
अपने छूटने की अर्जी के पीछे की भूमिका को स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने अपने भाई को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है। इस पत्र की विषय वस्तु तुरंत वर्तमान पत्र में छप गई जिसका संज्ञान पुलिस ने भी लिया। इसका पत्र का कुछ अंश दे रहे हैं।
पोर्ट ब्लेअर,
दिनांक ६-७-१९२०
प्रियतम बाल,
…बंदी मुक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया हैं। सैकडों बंदी कारागृह से मुक्त हो रहे हैं। विशेषकर जिन्होंने राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के लिए अनगिनत हस्ताक्षरों के आवेदनों की योजना बनाई और उसे बल दिया, उसके लिए जिन्होंने परिश्रम किए वे हमारे नेता और देशबंधु, उसमें भी मुख्यत बॉम्बे नेशनल यूनियन के अनवरत परिश्रम का ही यह फल हैं। इतनी छोटी अवधि में पौन लाख लोगों के नाम से भेजे गए आवेदन का सरकार के मन पर विलक्षण परिणाम हुआ ही होगा। फिर वे चाहे कितना ही अस्वीकार करें। कम-से-कम इस आवेदन के राजनीतिक बंदियों की और उसके कारण जिस कार्य के लिए वे लडे और हारे, उस कार्य की नैतिक प्रतिष्ठा बढी हैं, इसमें कोई शंका नहीं। अब सचमुच में हमारी मुक्ति होती ही हैं, तो उसमें कुछ सार दिखाई देगा, क्योंकि हम उनमें लौट आए ऐसी इच्छा हमारे देशबंधुओं ने प्रदर्शित की हैं। उन्होंने हमारे लिए जो चिंता और सहानुभूति प्रदर्शित की उसके लिए कितना भी आभार हम व्यक्त करें, कम ही रहेगा। उनकी जितनी आत्मीयता और आदर्श हमारे लिए दिखाया हैं और उनके प्रयास बिलकुल व्यर्थ ही नहीं गए। क्योंकि यद्यपि हम दोनों इस क्षमादान की सीमा के बाहर हैं, ऐसा कहा गया हैं, और उस कारण हमें उस कोठरी में सडते रहना पड रहा हैं, फिर भी हमारे साथ कष्ट भोगे हुए और राजनीति में हमसे सहकार्य किए हुए सैकडों देशभख्तों की मुक्ति के दृश्य से हमारे कष्ट हमें कुछ हलके से लगते हैं और इस कारण गत आठ वर्ष यहाँ और अन्य स्थानों पर हडताल, पत्र, आवेदन आदि के द्वारा समाचारपत्रों से या मंचों से जो आंदोलन हमने चलाए उसका फल मिलने का हमें संतोष है।
…दिनांक 2.4.1920 को मैंने शासनकर्ताओं द्वारा अभी हाल में दिए गए क्षमादान के प्रश्न पर एक नया आवेदन सरकार को भेजा हैं। उस आवेदन में सरकार ने जो सैकडों राजनीतिक बंदी छोडे, उसके लिए तथा इस तरह मेरा सन् 1917 का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया, इसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त किए हैं। और फिर अब भी बंधन में रखे गए और उसी तरह राजनीतिक कारण से परदेश में अटके हुए लोगों को भी लाभ मिले, इस रीति से इस क्षमादान की मर्यादा बढनी चाहिए – ऐसा निवेदन भी किया।
…सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदला हैं और भारतवर्ष को स्वतंत्रता, समर्थता और पूर्ण चैतन्य के मार्ग से सशस्त्र प्रतिकार न करते हुए आगे बढाने की उसकी इच्छा हैं, यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई हैं। मेरा विश्वास हैं कि सचमुच ऐसी परिस्थिति हो ते मेरे जैसे ही अन्य भी बहुत से क्रांतिकारी अपने कदम जहाँ – के – तहाँ रोक लेंगे। इन प्राफ्त सुधारों के बाद की विधानसभा के टूटे-फूटे रास्ते की धर्मशालाओं में मानप्रद करार के लिए इंग्लैंड से हाथ मिलाने को तैयार होंगे और प्रगति के रास्ते पर पुन आगे पैर बढाने का आदेश होने तक वहाँ काम भी करेंगे।
…इसलिए, हम जो क्रांतिकारी हुए वे निरूपाय होकर हुए हैं, उल्लास से नहीं। हिंदुस्थान के वास्तविक हित की दृष्टि से और इंग्लैंड के भी हित की दृष्टि से एक दूसरे के सहयोग, सहकार्य एवं शांति से और क्रमश प्रगति करते हुए अपना ध्येय प्राफ्त करना उन्हें आवश्यक हैं, ऐसा हमें तब भी लगता था और अब भी यदि वह आवश्यक हो तो शांति के उपायों का अवलंबन करने के लिए प्राप्त पहले अवसर का लाभ मैं लूँगा और प्रत्यक्ष क्रांति से या अन्य रास्तों से बनी घटनानुसार प्रगति के दरार में, फिर वह कितनी ही संकुचित हो, घुस जाऊँगा और उक्रांति की सेना उसमें से निरंतर, बाधारहित रूप से जा सके, इस रीति से वह दरार चौडी करने का प्रयास करूँगा।
सरकार यदि संविधान में पूरे मन से सुधार कर उन्हें लागू भी करती हैं और उन सुधारों से वह दरार बनी तो फिर राज्यक्रांति वहीं समाप्त हो जाएगी। उसके स्थान पर उत्क्रांती शब्द हम सबमें एकता उत्पन्न करनेवाली गर्जना तथा संकेत का शब्द होकर रहेगा और मातृभूमि की सेना के एक क्षुद्र सैनिक के रूप में वह सुधार सफल करने के कार्य में पूरे मन से मैं जुट जाऊँगा, जिससे वे सुधार भारतवर्ष के पुन वैभवशाली और महान् बनाने एवं अन्य राष्ट्रों के हाथ अपने हाथ में लिये या उन्हें रास्ता दिखाते हुए मनुष्य जाति के (उज्जवल) भविष्य की ओर ले जाने का अपनी पीढी का महान् कार्य पूरा करने के रास्ते पर कदम रखने का एक स्थान वह बने – इस रीति के उसका उपयोग कर लूँगा।
…इस आवेदन से हमारे छूटने के संबंध में विशेष कुछ होगा, ऐसी आशा मत करना। हमने अपनी आशा कभी भी बढने नहीं दी। इसीलिए न छूटने पर हमें उस संबंध में खास निराश भी नहीं होगी। कुछ भी फैसला हो, हम उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। तुमने अपनी और से यथासंभव प्रयास किए और मुख्यत तुम्हारे सतत परिश्रम का ही यह फल हैं कि राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के प्रश्न को इतना तीव्र स्वरूप मिला, यद्यपि हम दोनों को नहीं छोडा गया तो भी शेष सैकडों राजनीतिक बंदियों को स्वतंत्रता प्राफ्त हुई हैं।
तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम होगा, ऐसी आशा करते हुए और अपने स्नेही और रिश्ते-नातेदारों को नमस्कार लिखकर यह पत्र पूरा कर रहा हूँ।
तुम्हारा ही प्रिय बंधु,
तात्या।